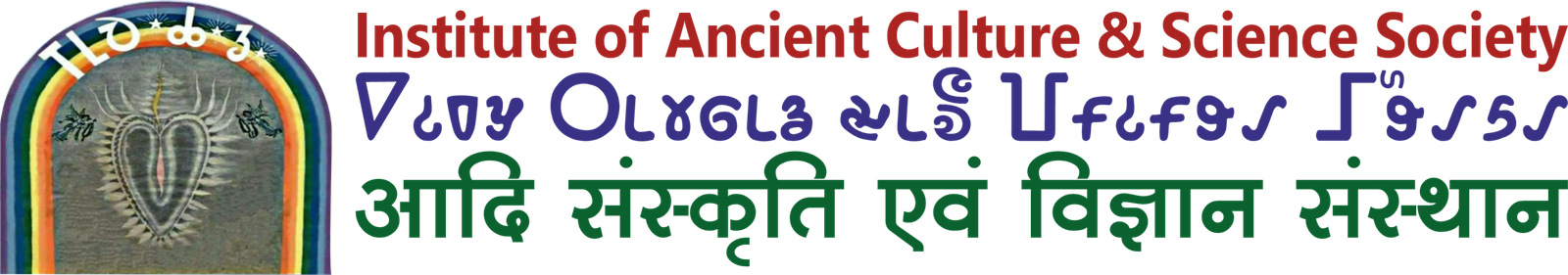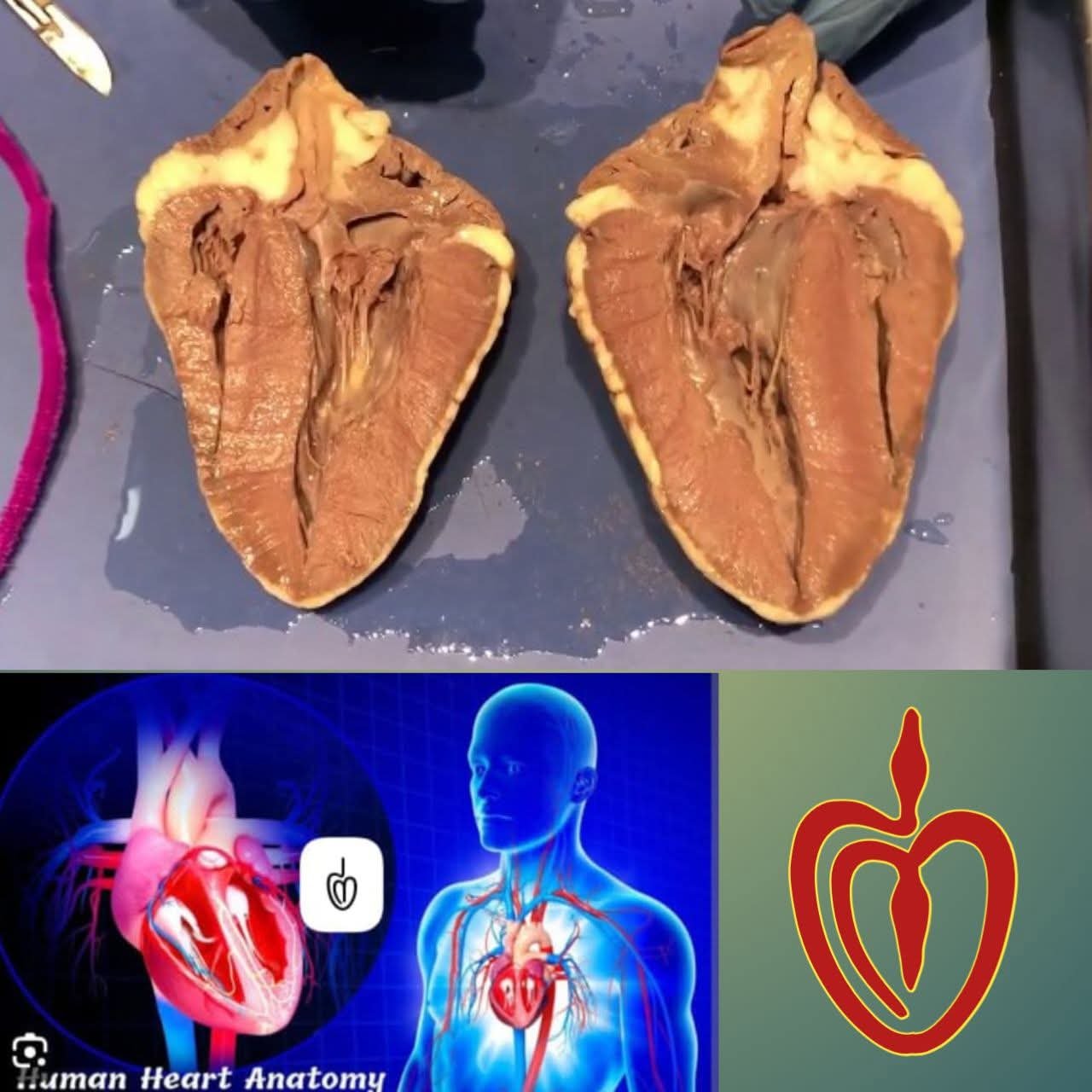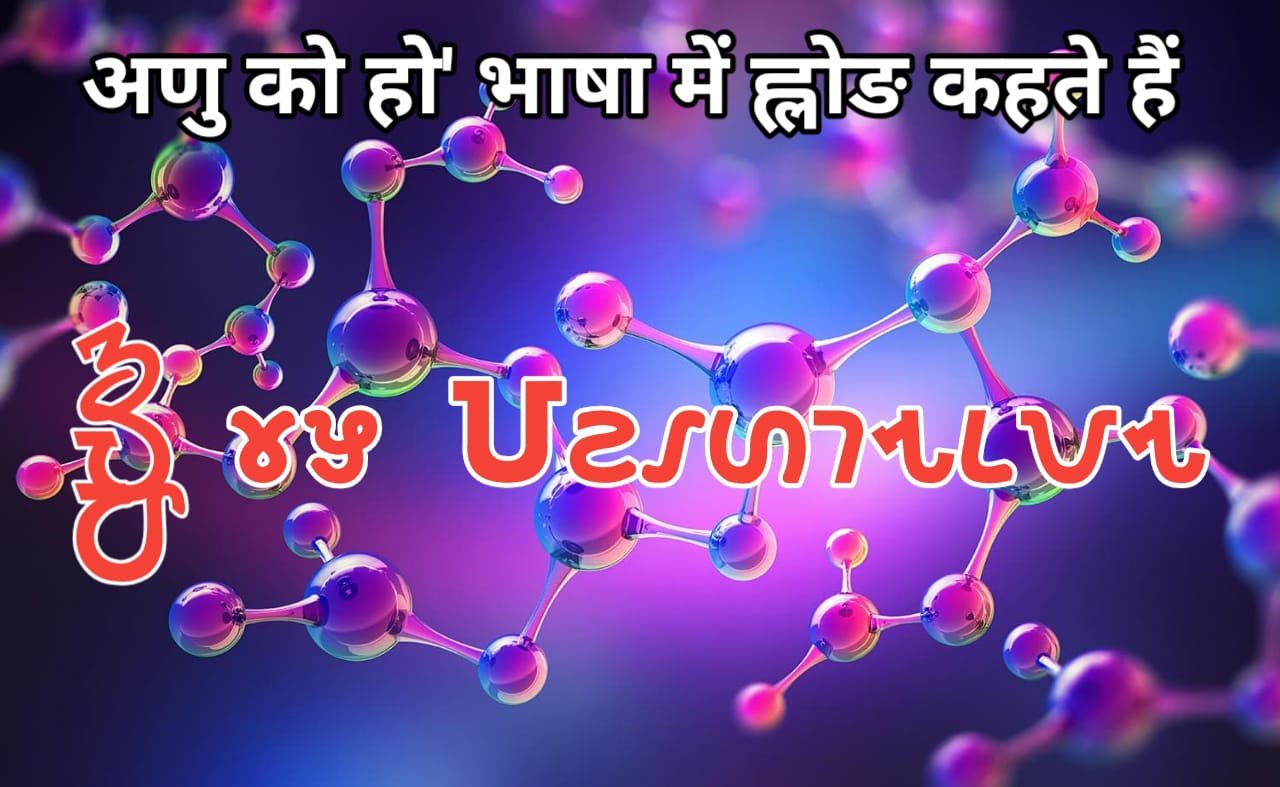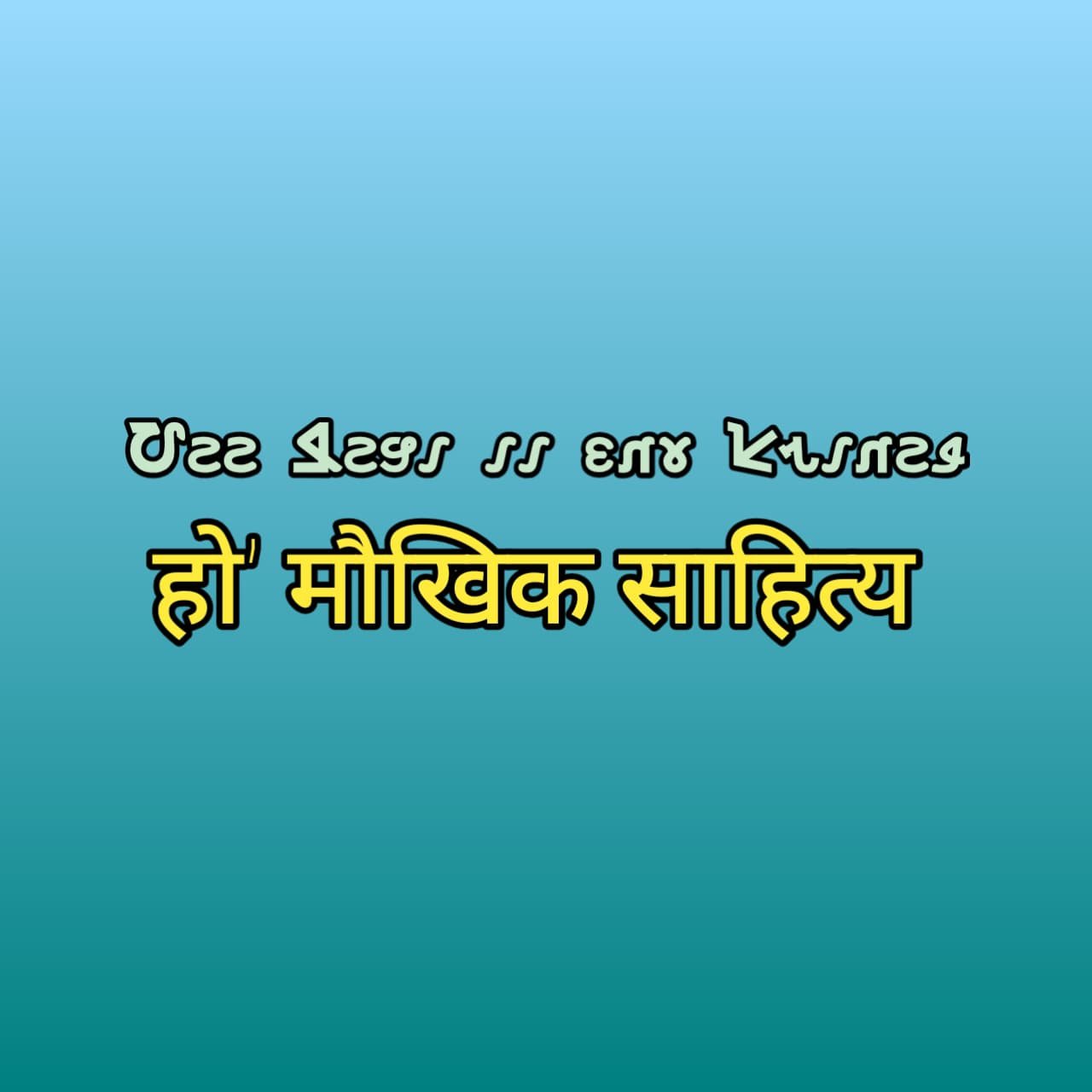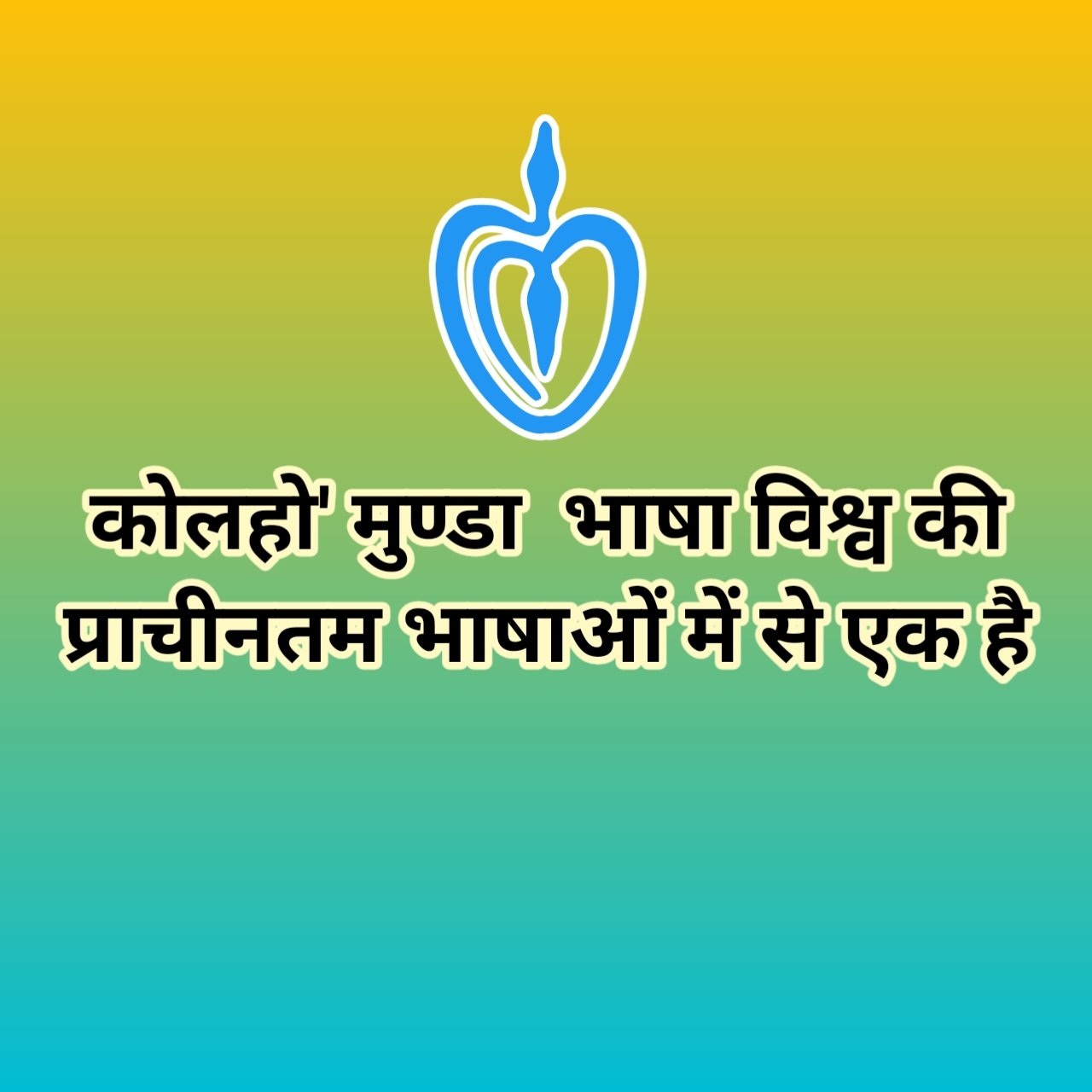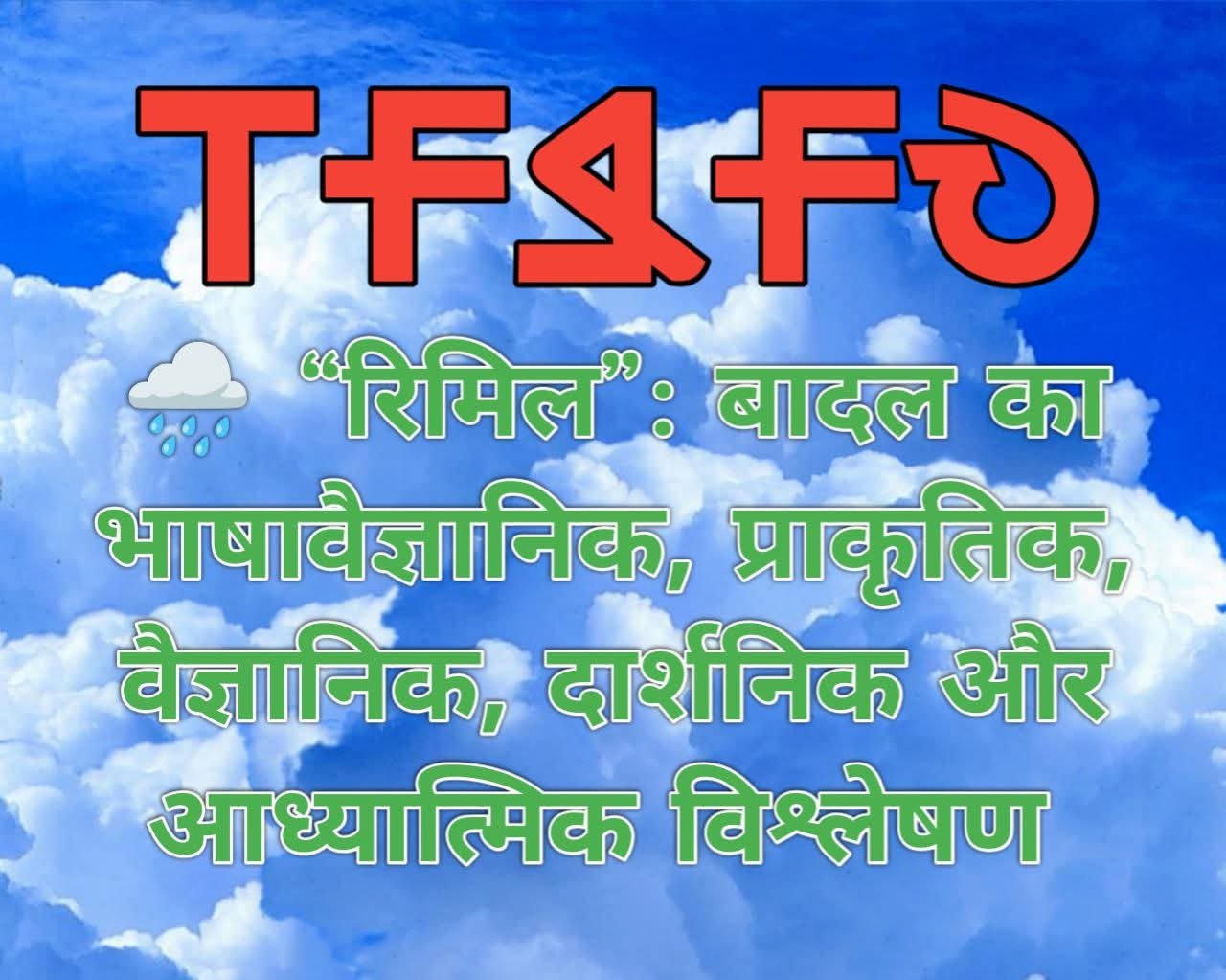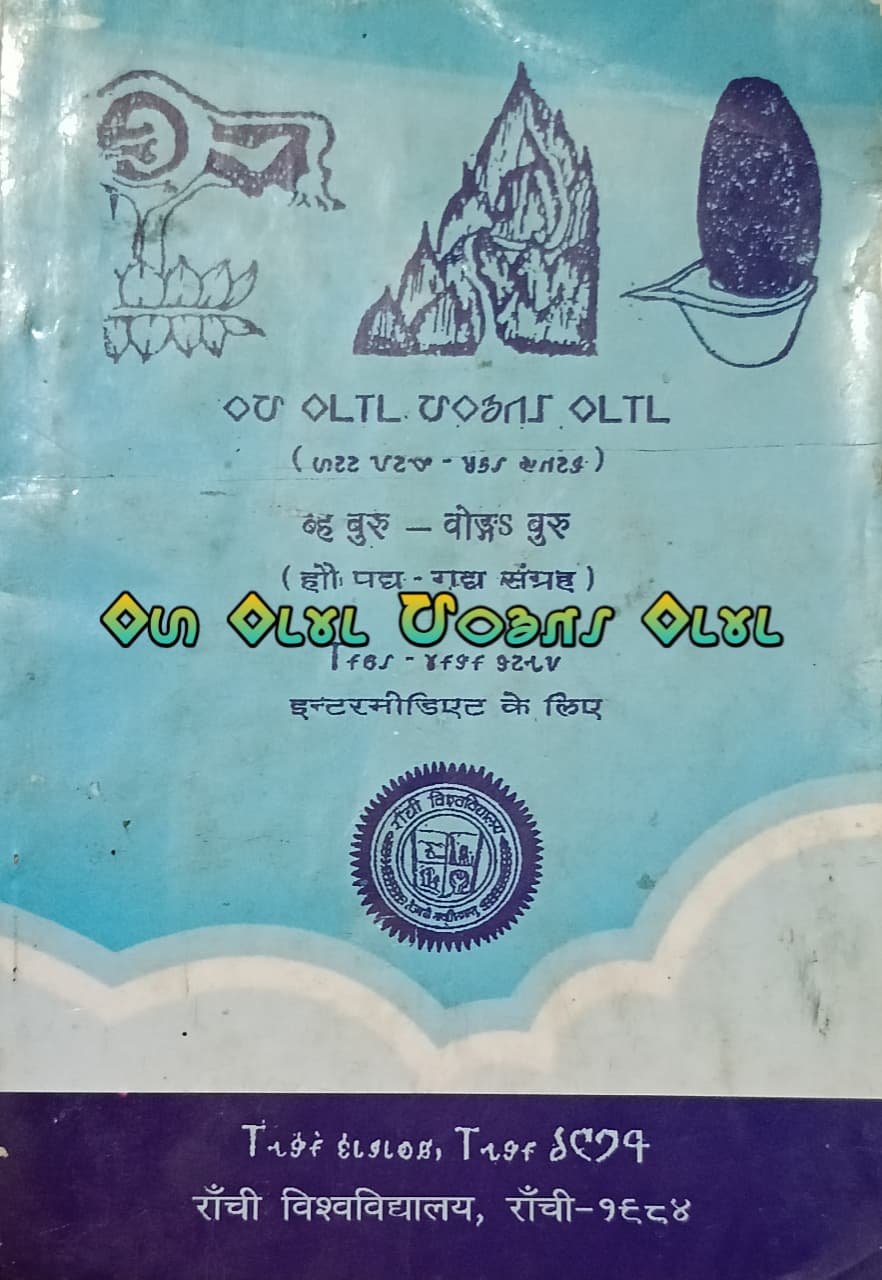ho maukhik saahity हो’ मौखिक साहित्य :
ho maukhik saahity किसी भी क्षेत्र, जाति या जनजाति के लोक साहित्य की मौखिक परम्परा अनादि काल से चलती आती है। हम जानते हैं कि वेदकालीन ऋचाओं की एक लम्बी मौखिक परम्परा रही है और इसी कारण वेदों को “श्रुति” भी कहा गया है। उसी प्रकार विभिन्न जनजातियों की लोक कथाओं, लोक गीतों, पहेलियों आदि का प्रचलन, विकास और विस्तार मौखिक रूप से ही होता रहा है। मौखिक परम्परा का कारण ‘लिपि’ की उत्पत्ति और विकास से भी सम्बन्धित है। लिपि के अभाव में ही आदिमानव द्वारा अंग संचालन और अन्य ध्वनि संकेतों से आपस में संवादों का सम्प्रेषण हुआ करता था। बाद में चित्र लिपि का विकास ‘शैलीचित्रों’ के रूप में हुआ, जिसे लिपि का आदि स्वरूप माना जाता है। ‘वारचिक्ति’ के अध्याय में लिपि के विकास और विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। यह भी सही है कि लिखित साहित्य के साथ-साथ लोक साहित्य की मौखिक परम्परा भी अनवरत चलती रहती है, जिसका संरक्षण नानी-दादी या बूढ़ा-बूढ़ी द्वारा सुनायी जाने वाली दंत कथाओं’ या मौखिक कथाओं के रूप में होता रहता है। आज भी अनेक कथाएं, गीत, कहावत एवं मुहावरे, पहले या बुझौलिया आदि का लिखित साहित्य के रूप में अभिलेखीकरण नहीं हो पाया है। लोक साहित्य की यह मौखिक परम्परा अनवरतरूप से कथक्कड़ों या कलाकारों के माध्यम से अक्षुण्ण बनी रहती है। ‘हो’ क्षेत्र में भी अनेकों ऐसे बूढ़े-बुजुर्ग हैं, जिनकी दन्तकथाएं उनके स्मृति पटल पर ही अंकित है और उसका अभिलेखीकरण या लेखन कार्य नहीं हुआ है, ऐसी मान्यता है।
‘हो’ मौखिक साहित्य या लोक साहित्य को आधार बनाकर रिजले, डाल्टन, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. राय आदि द्वारा बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उन्हें विभिन्न पुस्तकों और पत्रिकाओं में संकलित कर प्रस्तुत किया गया। उस अवधि में स्व. कानूराम देवगम ने अनेक लोक कथाओं और लोकगीतों को प्रस्तुत किया, जो अब दुर्लभ हैं। हो मौखिक साहित्य के अक्षुण्ण रहने और लोकजीवन में विकसित होने का कारण उनका हजारों वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन एवं प्रवर्जन भी रहा है। किसी भी साहित्य के लिखित रूप के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिरता एवं उनका विकास आवश्यक होता है। कोल्हान क्षेत्र में आकर बसने के बाद ही ‘हो लोक’ साहित्य के लिखित रूप का विकास परिलक्षित होता है। हो मौखिक साहित्य में अनेकों मिथक, धर्मगाथा, गोत्र कथा, परिकथा, मूर्खकथा आदि प्रचलित रही हैं। ‘सेंगेलगमा’ (आग की वर्षा या अग्नि प्रलय), सिबोंगा का टुअरकोड़ा-कसरा कोड़ा के रूप में अवतार लेने का मिथक, मानव विकास के प्रारम्भिक अवस्था में सुरमि-दुरभि नामक अर्ध विकसित मानव का सृजन आदि मिथकों का काफी बाद में देवनागरी लिपि के माध्यम से संकलन किया गया है। ‘हो’ जनजाति के विभिन्न गोत्रों का नामकरण वनों में उनके प्रवासकाल में ही किया गया। जिसका पशु-पक्षी, फल-फूल, नदी-झरना आदि से उनकी जीवन-रक्षा हई अथवा वंश वृद्धि में सहायक सिद्ध हुए, उनको गोत्र का प्रतीक बनाकर गोत्र का नाम रखा गया। वनों में घूमने के क्रम में उनके बीच अनेकों पशु-पक्षी कथा, प्रेत कथा, परी कथा आदि का जन्म मौखिक परम्परा से ही हुआ होगा। कालान्तर में विभिन्न विद्वानों द्वारा उन्हें पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से लिखित साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर गाये जाने वाले गीतों, भजनों, गोवारी या प्रार्थना आदि की भी एक लम्बी मौखिक परम्परा रही है। आज भी अनेक पर्व, गीत, विवाह गीत आदि मौखिक परम्परा के कारण ही जीवित है, और लोकप्रिय हैं। इन गीतों में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। विभिन्न ताल-लय पर गाये जाने वाले गीत आदि काल से ‘हो’ समाज में प्रचलन में हैं। सिन्धुघाटी तथा अन्य स्थानों/गढ़ों में निवास करने और उस समय की सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन पद्धति का संकेत एवं उल्लेख उन लोक गीतों में मिलता है। इस प्रकार के वर्णन ‘हो’ के साथ-साथ ऑस्ट्रिक समुदाय की सभी जनजातियों के गीतों में मिलते हैं। इन गीतों का एक वृहत् संकलन सी.एच. बोम्पास द्वारा संकलित ‘हो दुरंग’ शीर्षक पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसमें माघे, हेरो, जोमनामा आदि पर्वों के लम्बे-लम्बे गीत संकलित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे मौखिक गीतों को लिपिबद्ध कर प्रस्तुत किया जाता रहा है।
पूजा-पाठ और झाड़-फूंक के अवसर पर प्रयुक्त किये जाने वाले मंत्र गुप्त माने जाते हैं। जनजातीय समुदाय में तंत्र-मंत्र का लोक विश्वास काफी प्रचलित रहा है। हो ‘दिउरी’ (पुजारी) द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रयोग में लाये जानेवाले अनेकों मंत्र अभी भी मौखिक परम्परा में ही जीवित हैं। कतिपय मंत्रों का संग्रह डॉ. सतीश कुमार कोड़ा: ‘सेंगेल’ द्वारा ‘सतीश तन्त्र संहिता’ शीर्षक पुस्तक में किया गया है। उसी प्रकार ‘हो’ समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, लोकोक्ति आदि का संकलन ‘हो दिशुम हो होन को’ शीर्षक पुस्तक के विभिन्न खंडों (७ खंडों) में देवनागरी लिपि और हो भाषा के माध्यम से धनुर सिंह पुरती द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
अतः हो साहित्य की मौखिक परम्परा की जड़ें काफी गहरी हैं और उन्हें सम्पूर्ण रूप से लिखित परम्परा में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हो साहित्य की मौखिक परम्परायें कोयल-कारों की वेगवती जल-धारा की तरह निरन्तर गतिमान रहेंगी, एक दूसरे से पोषित और संवर्धित होती रहेंगी।
स्रोत – हो भाषा और साहित्य का इतिहास
लेखक – डॉ आदित्य प्रसाद सिन्हा